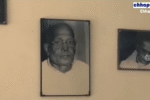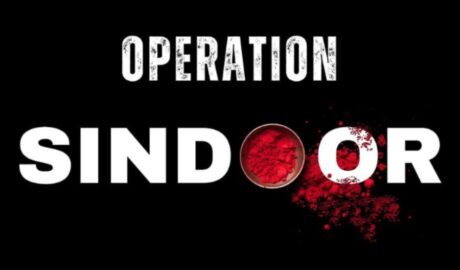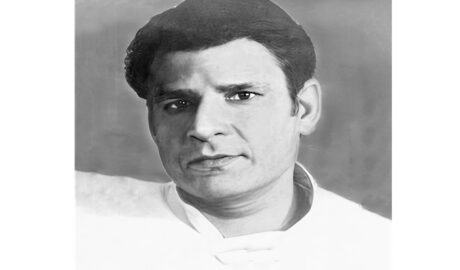जयप्रकाश नारायण जन्मदिवस विशेष: सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है
(डॉ प्रशांत सिन्हा) मेरे पिताजी अक्सर जयप्रकाश आंदोलन की चर्चा अपने मित्रों से करते थे और मैं उनके पास बैठ कर उनकी बातें सुना करता था। मेरा विद्यालय जयप्रकाश बाबू के घर के ठीक सामने था। मैं हमेशा उन्हें धूप में किताबें पढ़ते हुए देखा करता था। शिक्षकगण भी उनके विषय में चर्चा किया करते थे।
जयप्रकाश बाबू के घर पर देश विदेश के गणमान्य लोगों का आना जाना लगा रहता था। इससे अनजाने में ही जयप्रकाश बाबू में लगाव हो गया। उनके विषय में कहीं भी चर्चा होती थी मैं ध्यान से सुना करता था। उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा दिए गए नारा “ सम्पूर्ण क्रांति “ से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं राजनीति में नहीं हूँ लेकिन अछूता भी नहीं हूँ क्योंकि पटना या बिहार की राजनीति का तापमान हमेशा ऊँचा रहता है।
बिहार में राजनीतिक जागरूकता देश के दूसरे राज्यों से ज़्यादा है।ये सभी को मालूम है जयप्रकाश बाबू चिंतक भी थे और सामाजिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा भी थे कि इन्दिरा गांधी की सत्ता हिली ही नहीं वे ख़ुद भी हार गयीं। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। जयप्रकाश बाबू को विश्व के कोने कोने के लोग जानते थे।अपनी अपनी तरह से विचारकों ने उनका मूल्याँकन भी किया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सम्पूर्ण आंदोलन तक का जेपी का योगदान जगज़ाहिर है।
राजनीति एवं सत्ता दोनो अलग अलग है ये मैंने जयप्रकाश बाबू को थोड़ा जानने के बाद जाना। अधिकांश लोग राजनीति और सत्ता को एक मानते हैं। लोग राजनीति में आते हैं और सत्ता दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने इस नियम को तोड़ा। वे अपनी ज़िंदगी के आख़िरी क्षण तक राजनीति में रहें लेकिन सत्ता को ठुकराया। वे चाहते तो सत्ता के शिखर तक आसानी से पहुँच जाते। भारत के राजनीतिक आकाश पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ध्रुवतारे की तरह बने रहेंगे।
लोगों ने पूरे मन से उन्हें “लोकनायक” की उपाधि दी। वह ऐतिहासिक क्षण थी – 5 जून 1975 । जगह – पटना का गांधी मैदान । यह मैदान अनेक घटनाओं का जीता जागता गवाह है। पूरे बिहार से लोग विधान सभा भंग करने की माँग को लेकर पटना में जुटे थे। जेपी उस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। दस लाख से भी ज़्यादा लोगों की जुलूस थी। उस भीड़ से गांधी मैदान छोटा पड़ गया था। गांधी मैदान की सभा में उनके सिर पर लोगों ने “लोक नायक “ का ताज रख दिया जो हमेशा लगा रहा। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा था “ दोस्तों , ये संघर्ष सीमित उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा है। इसके उद्देश्य दूरगामी है। भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सूधृढ़ बनाना और जनता का सच्चा राज क़ायम करना है। एक नैतिक, सांस्कृतिक, तथा शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना और नया भारत बनाना है। यह सम्पूर्ण क्रांति है – टोटल रेवलूशन ( total revolution ) उसके बाद यह नारा निकला
“सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है ।
सम्पूर्ण क्रांति का अर्थ प्रत्येक दिशा में सतत विकाश ही समग्र क्रांति है।आचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, एवं शिक्षा में परिवर्तन कर के उन्हें जीवनपयोगि बनाने की आवश्यकता है। ग्राम स्तर से राष्ट्र स्तर तक जनसमिति एवं छात्र समिति बना कर छात्र जन-समस्याओं का निराकरण करते हुए तथा स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधियों को भेजना सुनिश्चित करना होगा।जन विरुद्ध कार्य करने पर प्रतिनिधि वापसी का अधिकार का उपयोग करते हुए उन्हें पदच्युत करना ताकि जनजीवन उन्नत एवं सरस बनाया जा सके।जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रांति के आंदोलन में अंतर्जातिय विवाह और जनेउ तोड़ने का कार्यक्रम अपनाया था। इसके साथ ही उन्होंने जाति और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करने के लिए लोगों को युवकों एवं युवतियों को संगठित करना शुरू कर दिया था।साथ ही बिना तिलक दहेज के सादगी के साथ शादी विवाह का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया था।
जयप्रकाश नारायण की दृष्टि में सम्पूर्ण क्रांति का अर्थ : सम्पूर्ण क्रांति का मतलब समाज में परिवर्तन हो – सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक,और नैतिक परिवर्तन।सामाजिक परिवर्तन ऐसा हो कि सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो। इसमें से नया समाज निकले जिसमें सभी सुखी हों।अमीर ग़रीब का जो आकाश पाताल का भेद है वह नहीं रहे। शोषण न हो इंसाफ़ हो।आर्थिक परिवर्तन ऐसा हो कि जो सबसे नीचे के लोग हैं जो सबसे ग़रीब हैं – चाहे वे किसी जाति या धर्म के हों ऊपर उठे।सांस्कृतिक परिवर्तन है – समाज में त्याग, बलिदान,प्रेम, अहिंसा, भाई चारा आदि सदगुणों का विकास करना।
जयप्रकाश शुरू से ही युवा हृदय सम्राट के रूप में विख्यात थे। नौजवानों की उनके ऊपर अटूट आस्था थी। इसी आस्था और प्यार के चलते अपने जीवन के चौथेपन में भी करोड़ों युवक, किशोरों का नेतृतव कर सके।आज के युवकों को लोक नायक जयप्रकाश की सम्पूर्ण क्रांति “ को समझने की आवश्यकता है